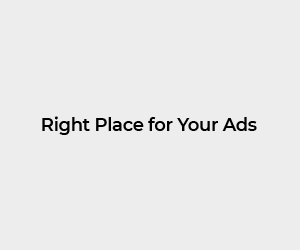सिनेमा को सिनेमा कहना बन्द कर देना चाहिए। खासकर हिंदी सिनेमा को। अब इसे सिर्फ़ मनोरंजन जगत ही कहना उपयुक्त होगा। पहले करोड़ों के बजट से फ़िल्म बनती है,फिर करोड़ों खर्च करके उसका प्रमोशन।
करोड़ों पानी की तरह बहते हैं। इस बहने और बहाने में न जाने कितने ऐसे मुद्दे बह जाते हैं,जिसकी समाज को बहुत जरूरत होती है। सिनेमा को हम किसी देश व लोकतंत्र का पांचवां अदृश्य स्तम्भ मान सकते हैं। जहां समाज मे अन्याय,अत्याचार,गरीबी,भुखमरी फैली हो वहां करोड़ों का व्यापार और उसमें भी मुनाफा की बात ठीक वैसी ही है,जैसे रोटी नही तो ब्रेड खाने की बात की जाय।
समाज का दर्पण कहलाने वाले सिनेमा में अब सामाजिक मुद्दे धूमिल होते जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखने पर ही कुछ छवियां नज़र आती हैं,वो भी किसी किसी को। सिनेमा की समझ रखने वाले ही ऐसा सोच पाते हैं कि उनको जमीन पर जाकर दृश्यों को कैद करना है,न कि स्टूडियो में क्रोमा बनाकर या आधुनिक स्पेशल इफ़ेक्ट जैसी तकनीकि का प्रयोग करके।
हाल ही में रिलीज हुई फ़िल्म ‘ब्रह्मास्त्र’ को लेकर लोगों की नज़र कमाई पर है। मेकर्स को भी चिंता सिर्फ मुनाफे की है,न कि इसकी यह फ़िल्म किस समाज को दिखाती है या फिर ये धरती पर रह रहे इंसानों के किस वर्ग को प्रभावित करेगी। खुशियां मनाई जा रही और जश्न मनाये जा रहे। मगर इस बीच दर्शकों का ध्यान ऐसी फिल्मों पर नही जा रहा जो उनको असल समस्या से मुखातिब करा पाए।
प्रकाश झा प्रोडक्शन से आ रही फिल्म ‘मट्टो की साइकिल’ पर कम ही दर्शकों की नज़र है,जबकि यह फ़िल्म देश के एक बड़े वर्ग की समस्या को इंगित करती कहानी पर है। इसका निर्देशक एक बड़े निर्देशक को जमीन पर ले जाता है। वह निर्देशक अभिनय करता है और जान भर देता है। उसके सर पर ईंट,गिट्टी,सरिया और बोरे का बोझ किसी स्पेशल इफ़ेक्ट से नही बल्कि असल रूप में दिखाया गया है। वह कीचड़ में गिरता है,माटी लपेट लेता है,बीड़ी फूंककर अपने गमों व चिंताओं को धुवें में उड़ाता है। ऐसी हज़ारों समस्याएं हैं जिनको मट्टो व मट्टो जैसे इंसान रोज झेल रहे हैं।
यह बात सच है कि सिनेमा बदल रहा है। मगर उतनी ही यह बात भी सच है कि समाज भी बदल रहा है। सिनेमा भले बदलकर आज चकाचौंध वाली दुनिया में प्रवेश कर चुका हो,मगर समाज से समस्याएं खत्म नही हुई हैं।
समाज की हमेशा से,सिनेमा से एक उम्मीद रही है। उस उम्मीद पर सिनेमा खरा उतर पा रहा है? यह दर्शकों को अपनी अंतरात्मा से सवाल जरूर करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम मनोरंजन करती फिल्में देखकर हंस लेते हैं,नाच लेते हैं,झूम लेते हैं। मगर क्या इसका कोई दूरगामी सकारात्मक परिणाम है या फिर नही?
सिनेमा दर्शक की आंखों पर एक पट्टी चढ़ा देता है,फिर दर्शक वही देखेगा जो वो दिखाना चाहता है। लेकिन सिनेमा में कम ही ऐसी फिल्में बन रही,जो दर्शक वर्ग को ठिठक कर खड़ा करने और उन्हें सोचने पर विवश कर दें। उनके भीतर एक प्रश्न छोड़ दें। और दर्शक उस प्रश्न का उत्तर तलाशे।